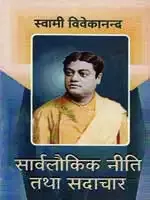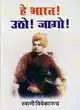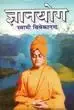|
विवेकानन्द साहित्य >> सार्वलौकिक नीति तथा सदाचार सार्वलौकिक नीति तथा सदाचारस्वामी विवेकानन्द
|
404 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है पुस्तक सार्वलौकिक नीति तथा सदाचार...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्रस्तावना
श्री स्वामी विवेकानन्दकृत ‘सार्वलौकिक नीति तथा
सदाचार’ का
संस्करण प्रकाशित करते हमें हर्ष हो रहा है। वस्तुत: यह ग्रन्थ स्वामीजी
के अनेक ग्रन्थों में से संकलन है। यह बात सर्वमान्य है कि विद्यालयों तथा
महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के जीवन-गठन तथा चरित्र-निर्माण के लिए
उन्हें नैतिक एवं अध्यात्मिक तत्त्वों की शिक्षा देना परमावश्यक है। इसी
उद्देश्य से प्रेरित होकर भारत सरकार ने श्रीप्रकाश की अध्यक्षता में एक
समिति का निर्माण किया जिसने इस बात की जाँच की कि शिक्षासंस्थाओं में
सदाचार तथा अध्यात्म संबंधी विषय के अध्ययन का समावेश कितना अधिक वांछित
है। फलत: इस समिति ने यह सिफारिश की कि भारत सरकार इस संबंध में ऐसी
उपयुक्त पाठ्यसामग्री एकत्रित कराये, जो विद्यालय-महाविद्यालय में पढ़ायी
जाय, तथा उसके प्रकाशन की व्यवस्था करे। तदनुसार भारत शासन ने
श्रीरामकृष्ण मिशन के स्वामी रंगानाथानन्दजी से एक ऐसी पुस्तक तैयार कर
देने के लिए प्रार्थना की श्री स्वामी विवेकानन्द के ग्रन्थों में से
सार्वलौकिक नीति तथा सदाचार संबंधी सामग्री संकलित हो। स्वामी रंगानाथनजी
ने मूल अग्रेजी से संकलन करके ऐसी पुस्तक तैयार कर दी और प्रस्तुत ग्रन्थ
उसी का हिन्दी अनुवाद है।
भारत सरकार ने इस बात की आवश्यकता समझी कि इस अंग्रेजी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो, जिससे अधिकाधिक विद्यार्थीसमाज लाभ उठा सकें। इसीलिए हम प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकाशित कर रहे हैं।
कहने की आवश्यकता नहीं, इस पुस्तक के अध्ययन से विद्यालय-महाविद्यालय के विद्यार्थियों और साथ ही सामान्य जनता को स्वामी विवेकानन्द के उदात्त एवं उत्थानकारी भावों का परिचय प्राप्त हो सकेगा तथा इसमें दी हुई सार्वलौकिक शिक्षाओं से विद्यार्थियों के जीवन का सर्वांगीण विकास हो उनके चरित्र-गठन में सहायता मिलेगी। साथ ही, इस पुस्तक के भाव सार्वलौकिक होने के नाते समस्त विद्यार्थी-संसार तथा सभी अन्य व्यक्तियों के लिए भी, वे किसी जाति अथवा धर्म के हों, समाज रूप से हितकारी होंगे।
हमें पूर्ण विश्वास है कि इस ग्रन्थ के पठन-पाठन से हमारे विद्यार्थियों को आदर्श नागरिक बनने में विशेष सहायता मिलेगी, साथ ही जीवन के विभिन्न पदों, अवस्थाओं तथा परिस्थितियों में उन्हें अपने कर्तव्य को पूर्णरूपेण निबाहने में पथप्रदर्शन प्राप्त होगा।
भारत सरकार ने इस बात की आवश्यकता समझी कि इस अंग्रेजी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो, जिससे अधिकाधिक विद्यार्थीसमाज लाभ उठा सकें। इसीलिए हम प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकाशित कर रहे हैं।
कहने की आवश्यकता नहीं, इस पुस्तक के अध्ययन से विद्यालय-महाविद्यालय के विद्यार्थियों और साथ ही सामान्य जनता को स्वामी विवेकानन्द के उदात्त एवं उत्थानकारी भावों का परिचय प्राप्त हो सकेगा तथा इसमें दी हुई सार्वलौकिक शिक्षाओं से विद्यार्थियों के जीवन का सर्वांगीण विकास हो उनके चरित्र-गठन में सहायता मिलेगी। साथ ही, इस पुस्तक के भाव सार्वलौकिक होने के नाते समस्त विद्यार्थी-संसार तथा सभी अन्य व्यक्तियों के लिए भी, वे किसी जाति अथवा धर्म के हों, समाज रूप से हितकारी होंगे।
हमें पूर्ण विश्वास है कि इस ग्रन्थ के पठन-पाठन से हमारे विद्यार्थियों को आदर्श नागरिक बनने में विशेष सहायता मिलेगी, साथ ही जीवन के विभिन्न पदों, अवस्थाओं तथा परिस्थितियों में उन्हें अपने कर्तव्य को पूर्णरूपेण निबाहने में पथप्रदर्शन प्राप्त होगा।
नागपुर
4.6.1997
4.6.1997
प्रकाशक
जब तक अन्यथा निर्देश न हो, परिच्छेदों के अन्त में दिये गये सन्दर्भ
स्वामी विवेकानन्दकृत हिन्दी पुस्तकों से हैं जो रामकृष्ण मठ, धन्तोली,
नागपुर-12 द्वारा प्रकाशित हुई हैं।
-प्रकाशक
सार्वलौकिक नीति तथा सदाचार
1
जीवन का सच्चा आधार
-नैतिकता और सच्चरित्रता
मनुष्य की साधुता ही सामाजिक तथा राजनीतिक सर्वविध व्यवस्था का आधार है।
पार्लमेन्ट द्वारा बनाये गये कानूनों से ही कोई राष्ट्र भला या उन्नत नहीं
हो जाता। वह उन्नत तब होता है, जब वहाँ के मनुष्य उन्नत और सुन्दर
स्वभाववाले होते हैं।
बहुधा लोग एक ही उद्देश्य से कर्म में प्रवृत्त होते हैं, पर वे यह समझ नहीं पाते। यह तो मानना ही पड़ेगा कि कानून, सरकार या राजनीति मानव-जीवन का चरम उद्देश्य नहीं है। इन सब के परे एक ऐसा चरम लक्ष्य है, जहाँ पहुँचने पर कानून या विधि का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता।......सभी महान् आचार्य यही शिक्षा देते हैं। ईसा मसीह जानते थे कि कानून का प्रतिपालन ही उन्नति का मूल नहीं है, बल्कि पवित्रता और सच्चरित्रता ही शक्तिलाभ का एकमात्र उपाय है।
बहुधा लोग एक ही उद्देश्य से कर्म में प्रवृत्त होते हैं, पर वे यह समझ नहीं पाते। यह तो मानना ही पड़ेगा कि कानून, सरकार या राजनीति मानव-जीवन का चरम उद्देश्य नहीं है। इन सब के परे एक ऐसा चरम लक्ष्य है, जहाँ पहुँचने पर कानून या विधि का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता।......सभी महान् आचार्य यही शिक्षा देते हैं। ईसा मसीह जानते थे कि कानून का प्रतिपालन ही उन्नति का मूल नहीं है, बल्कि पवित्रता और सच्चरित्रता ही शक्तिलाभ का एकमात्र उपाय है।
(स्वामी विवेकानन्द से वार्तालाप-पृ. 21-22)
(2)
विश्व की प्रेरक शक्ति
-प्रेम और त्याग
समस्त नैतिक अनुशासन का मूलमंत्र क्या है ? ‘नाहं नाहं, त्वमसि
त्वमसि (मैं नहीं, मैं नहीं-तू ही, तू ही)।’ हमारे पीछे जो
‘अनन्त’ विद्यमान है, उसने अपने बहिर्जगत् में व्यक्त
करने के
लिए इस ‘अहं’ का रूप धारण किया है। उसी से इस क्षुद्र
‘मैं’ की उत्पत्ति हुई है। अब इस
‘मैं’ को फिर
पीछे लौटकर अपने अनन्त स्वरूप में मिल जाना होगा। जितनी बार तुम कहते हो
‘मैं’ नहीं, मेरे भाई, वरन् तुम ही’ उतनी
ही बार तुम
लौटने की चेष्टा करते हो, और जितनी बार तुम कहते हो, ‘तुम नहीं,
‘मैं’, उतनी बार अनन्त को यहाँ अभिव्यक्त करने का
तुम्हारा
मिथ्या प्रयास होता है। इसी से संसार में प्रतिद्वन्द्विता, संघर्ष और
अनिष्ट की उत्पत्ति होती है। पर अन्त में त्याग-अनन्त त्याग का आरम्भ होगा
ही। यह ‘मैं’ मर जायगा। अपने जीवन के लिए तब कौन यत्न
करेगा ?
यहाँ रहकर इस जीवन के उपभोग करने की व्यर्थ वासना और फिर इसके बाद स्वर्ग जाकर इसी तरह रहने की वासना- अर्थात् सर्वदा इन्द्रिय और इन्द्रिय-सुखों में लिप्त रहने की वासना ही मृत्यु को लाती है।
.........हम हीन होकर पशु हो गये हैं। अब हम फिर उन्नति के मार्ग पर चल रहे हैं, और इस बन्धन से बाहर होने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर अनन्त को यहाँ पूरी तरह अभिव्यक्त करने में हम कभी समर्थ न होंगे। हम प्राणपण से चेष्टा कर सकते हैं, परन्तु देखेंगे कि यह असम्भव है। अन्त में एक समय आयगा, जब हम देखेंगे कि जब तक हम इन्द्रियों में आबद्ध हैं, तब तक पूर्णता की प्राप्ति असम्भव है। तब हम अपने मूल अनन्त स्वरूप की ओर वापस जाने के लिए पीछे लौट पड़ेंगे।
इसी लौट आने का नाम है त्याग। तब, हम इस जाल में जिस प्रक्रिया द्वारा पड़ गये थे, उसको उलटकर इसमें से हमें बाहर निकल आने होगा- तभी नीति और दया-धर्म का आरम्भ होगा।
यहाँ रहकर इस जीवन के उपभोग करने की व्यर्थ वासना और फिर इसके बाद स्वर्ग जाकर इसी तरह रहने की वासना- अर्थात् सर्वदा इन्द्रिय और इन्द्रिय-सुखों में लिप्त रहने की वासना ही मृत्यु को लाती है।
.........हम हीन होकर पशु हो गये हैं। अब हम फिर उन्नति के मार्ग पर चल रहे हैं, और इस बन्धन से बाहर होने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर अनन्त को यहाँ पूरी तरह अभिव्यक्त करने में हम कभी समर्थ न होंगे। हम प्राणपण से चेष्टा कर सकते हैं, परन्तु देखेंगे कि यह असम्भव है। अन्त में एक समय आयगा, जब हम देखेंगे कि जब तक हम इन्द्रियों में आबद्ध हैं, तब तक पूर्णता की प्राप्ति असम्भव है। तब हम अपने मूल अनन्त स्वरूप की ओर वापस जाने के लिए पीछे लौट पड़ेंगे।
इसी लौट आने का नाम है त्याग। तब, हम इस जाल में जिस प्रक्रिया द्वारा पड़ गये थे, उसको उलटकर इसमें से हमें बाहर निकल आने होगा- तभी नीति और दया-धर्म का आरम्भ होगा।
(ज्ञानयोग-पृ. 288)
सब प्रकार की नीति, शुभ तथा मंगल का मूलमंत्र ‘मैं’
नहीं,
‘तुम’ है। कौन सोचता है कि स्वर्ग और नरक हैं या
नहीं, कौन
सोचता है कि आत्मा है या नहीं, कौन सोचता है कि अनश्वर सत्ता है या नहीं ?
हमारे सामने यह संसार है और वह दु:ख से परिपूर्ण है। बुद्ध के समान इस
संसार-सागर में गोता लगाकर या तो इस संसार के दु:ख को दूर करो या इस
प्रयत्न में प्राण त्याग दो। अपने को भूल जाओ; आस्तिक हो या नास्तिक,
अज्ञेयवादी ही हो या वेदान्ती, ईसाई हो या मुसलमान, प्रत्येक के लिए यही
सबसे पहली शिक्षा है। यह शिक्षा, यह उपदेश सभी समझ सकते हैं,-
‘मैं
नहीं, मैं नहीं, तुम ही हो, तुम ही हो’- क्षुद्र
‘अहं’
का नाश और प्रकृति आत्मा का विकास।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book